 |
| उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना Geographical structure of Uttarakhand |
उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना | Geographical structure of Uttarakhand
शिलालेखीय विवरणों और चौरस
ताम्रपत्रों में उत्तराखण्ड के लिए ‘पर्वताकार-राज्य’ शब्द का प्रयोग हुआ है।
पाणिनी और कौटिल्य ने ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र तथा पाटलिपुत्र से वाहिक–कपिशा
जाने वाले मार्ग को उत्तरापथ नाम से संबोधित किया है। संभवतः कालांतर में
उत्तर भारत के लिए ‘उत्तरपथ’ या ‘उत्तरापथ’ नाम का प्रयोग होने लगा।
पौराणिक साहित्य में, हरिद्वार से लेकर महाहिमालय तक तथा टौंस नदी से
बौद्धाचल तक के क्षेत्र को केदारखण्ड और उससे पूर्व की ओर काली–शारदा नदी तक के क्षेत्र को मानखण्ड कहा गया है।
इन विभिन्न नामों से कोई निश्चित
निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता, परंतु
यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उत्तरापथ के ‘उत्तरा’ और केदारखण्ड के ‘खण्ड’ शब्द के संयोग से ‘उत्तराखण्ड’ नाम की उत्पत्ति हुई होगी।
उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमाएँ
भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तराखण्ड का
क्षेत्र भावर से लेकर हिमाचल तक तथा टौंस–यमुना से लेकर काली–शारदा तक विस्तृत है।
उत्तराखण्ड में कुमाऊँ मण्डल के छह जनपद — नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत और अल्मोड़ा — सम्मिलित हैं। गढ़वाल मण्डल के जनपद — देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी — भी इसमें आते हैं।
इसके अलावा सहारनपुर मण्डल का हरिद्वार जनपद भी उत्तराखण्ड में सम्मिलित किया गया
है।
गढ़वाल मण्डल हिमालय के केन्द्रीय
भाग में स्थित है। इसकी तलहटी में ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून के तराई और भावर
क्षेत्र हैं।
कुमाऊँ की दक्षिणी सीमा भावर–तराई
प्रदेश तक फैली है, जबकि काली–शारदा नदी अति प्राचीन काल
से राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की सीमा रही है। पश्चिम की ओर गढ़वाल राज्य
की सीमा पहले सहारनपुर के उत्तरी भाग तक विस्तृत थी। गढ़वाल राज्य की पश्चिमी सीमा
टौंस–यमुना की पश्चिमी घाटी तक, हिमाचल
प्रदेश में सतलुज के पूर्वी तट तक, और दक्षिण–पश्चिम में दृश्यद्वती तथा सरस्वती नदियों के स्रोत
प्रदेशों तक फैली हुई थी।
इस प्रकार उत्तराखण्ड की सीमाओं के
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का संपूर्ण उत्तर पर्वतीय भाग आता है, जो तराई–भावर की पट्टी से आरम्भ होकर भारत–तिब्बत
सीमांत तक तथा यमुना–टौंस की पश्चिमी घाटी से लेकर शारदा नदी तक फैला हुआ है।
स्थिति एवं विस्तार
उत्तराखण्ड का अक्षांशीय विस्तार 28°43' उत्तरी अक्षांश से 31°27' उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतर विस्तार 77°34' पूर्वी देशांतर से 81°02' पूर्वी देशांतर तक है। इसका कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी
कुल जनसंख्या 1,00,86,292 है, जिससे यह देश का 20वां बड़ा राज्य है।
प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखण्ड में
कुल 13 जिले आते हैं:
1. अल्मोड़ा
2. पिथौरागढ़
3. देहरादून
4. पौड़ी गढ़वाल
5. चमोली
6. नैनीताल
7. टिहरी गढ़वाल
8. उत्तरकाशी
9. ऊधमसिंह नगर
10.
बागेश्वर
11.
चम्पावत
12.
रुद्रप्रयाग
13.
हरिद्वार
उत्तराखण्ड की भूगर्भिक संरचना
उत्तराखण्ड का धरातलीय स्वरूप इसकी भूगर्भिक
संरचना से गहरे रूप में प्रभावित है। इस क्षेत्र की चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन
कई भूवैज्ञानिकों ने किया —
- मिडलमिस
(Middlemiss), 1887
- ग्रीसवैक
(Griesbach), 1891
- मेडलीकॉट
(Medlicott), 1864
- ए.
हाइम (A. Heim),
1931
ए. हाइम ने उत्तराखण्ड
की भूगर्भिक संरचना को 5 प्रमुख
पेटियों (Belts) में
विभाजित किया —
1.
स्वस्थानिक मेखला (Autochthonous Belt) — दून घाटी से
लगभग 50 किमी
उत्तर तक फैली हुई। यहाँ चूना पत्थर एवं निक्षेपित अवसाद मिलते हैं। इस क्षेत्र
में वलन (Folding) और
भ्रंशन (Faulting) अपेक्षाकृत
कम हैं।
2.
क्रोल नाप्पे (Krol Nappe) — देहरादून जिले
की चकराता तहसील के पूर्व भाग में स्थित।
3.
गढ़वाल नाप्पे (Garhwal Nappe) — क्रोल नाप्पे
के ऊपर स्थित, इसमें
आग्नेय शैलों (Igneous
Rocks) की प्रधानता है।
4.
मुख्य हिमालय मेखला (Greater Himalayan Belt) — गढ़वाल नाप्पे
की आधारशिला, जिसमें
ग्नीश (Gneiss) एवं
आग्नेय शैलों का आधिक्य है।
5.
मध्य समस्थानिक पेटी (Central Metamorphic Belt) — ग्रेनाइट, ग्नीश और शिस्ट
शैलों से निर्मित।
उत्तराखण्ड की पर्वत श्रेणियाँ
उत्तराखण्ड का अधिकांश भाग पर्वतीय है। तराई-भावर
क्षेत्र और दून घाटियों को छोड़कर शेष क्षेत्र चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित
है —
1.
शिवालिक या बाह्य हिमालय (Shivalik Range)
o ऊँचाई:
750–1200 मीटर
o औसत
वर्षा: ~40 इंच
o ढाल:
दक्षिण में तीव्र, उत्तर
में दून घाटी की ओर सरल
o दून
घाटियाँ: देहरादून, कोटीदून, चौखम्भा पट्टी, कोटा
o नदियाँ:
गंगा, यमुना, काली नदी
प्रणालियाँ
o विशेषताएँ:
हिमोढ़ निक्षेप (Glacial
Deposits), झीलें, नदी-चबूतरे
2.
मध्य हिमालय (Middle Himalaya)
o ऊँचाई:
1500–2700 मीटर
(कहीं-कहीं 3000 मीटर
तक)
o चौड़ाई:
~75 किमी
o भू-रचना:
Boundary Thrust द्वारा
शिवालिक से अलग
o प्रमुख
डांडे और चोटियाँ: मसूरी,
नागटिब्बा, चीनी शिखर, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल
3.
महाहिमालय या हिमाद्रि (Greater Himalaya)
o ऊँचाई:
6000–7800 मीटर
o प्रमुख
शिखर: नन्दा देवी, कामेत, चौखम्भा, त्रिशूल
o हिमपात:
ऊँचे क्षेत्रों में 120 इंच तक
वार्षिक वर्षा, सर्दियों
में बर्फ़बारी
4.
जंस्कार श्रेणियाँ (Zanskar Range)
o स्थिति:
भारत-तिब्बत सीमांत
o विशेषताएँ:
हिमनद (Glaciers), उच्च
पर्वतीय चरागाह
प्रमुख पर्वत शिखर
|
क्रम |
पर्वत शिखर |
ऊँचाई (मीटर) |
जनपद |
|
1 |
नन्दा देवी |
7,816 |
चमोली |
|
2 |
कामेत |
7,756 |
चमोली |
|
3 |
नन्दा देवी (पूर्वी) |
7,434 |
चमोली |
|
4 |
माणा |
7,273 |
चमोली |
|
5 |
चौखम्बा |
7,138 |
चमोली |
|
6 |
त्रिशूल |
7,120 |
चमोली |
|
7 |
द्रोणागिरि |
7,066 |
चमोली |
|
8 |
पंचचूली |
6,904 |
पिथौरागढ़ |
|
9 |
नन्दाकोट |
6,861 |
बागेश्वर |
|
10 |
बंदरपूँछ |
6,315 |
उत्तरकाशी |
हिमाद्रि या महाहिमालय श्रेणियाँ
हिमाद्रि पर्वत श्रेणियाँ लगभग 25–30 किमी चौड़ी हैं, जिनकी ऊँचाई 4,800 से 9,000 मीटर के बीच
है।
मुख्य
शिखर:
- वंदरपूँछ
– 6,315 मीटर
- गंगोत्री
– 6,614 मीटर
- केदारनाथ
– 6,940 मीटर
- चौखम्भा
– 7,138 मीटर
- कामेट
– 7,756 मीटर
- नंदा
देवी – 7,816 मीटर
- द्रोणागिरि
– 7,066 मीटर
- त्रिशूल
– 7,120 मीटर
- नंदाकोट
– 6,861 मीटर
इन शिखरों को भागीरथी, अलकनंदा और
धवली गंगा की नदी घाटियाँ अलग करती हैं। यह क्षेत्र गारनेट, क्वार्टजाइट और
नीस जैसी कठोर चट्टानों से बना है।
वनस्पति:
दक्षिणी
ढालों पर 10,000 फीट तक
चीड़, देवदार, बुरांस, खरसू, भीडू और
कहीं-कहीं भोजपत्र के सुंदर वन पाए जाते हैं। 12,000 फीट से ऊपर बुग्याल (घास के मैदान)
मिलते हैं और हिमरेखा के पास वनस्पति समाप्त हो जाती है।
जंस्कर श्रेणियाँ
महाहिमालय की उत्तरी ढालों से आगे, भारत-तिब्बत
सीमांत तक जंस्कर श्रेणियाँ फैली हैं।
मुख्य
दर्रे: जेलूखगा, माणा, नीति, चौरहोती, दमजन, शलशल, कुंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख।
मुख्य हिमानियाँ (ग्लेशियर):
- गंगोत्री
– 4,000–6,902 मीटर
(उत्तरकाशी)
- मिलाम
– 4,242 मीटर
(पिथौरागढ़)
- पोर्टिंग
– 3,650 मीटर
(पिथौरागढ़)
- नामिक
– 4,830 मीटर
(पिथौरागढ़)
- पिण्डारी
– 3,352–4,625 मीटर
(बागेश्वर)
- सुन्दरढूंगा
– 6,053 मीटर
(बागेश्वर)
- कफनी
– 3,840 मीटर
(बागेश्वर)
उत्तराखण्ड के प्रमुख दर्रे
|
क्रम |
दर्रा |
संपर्क क्षेत्र |
|
1 |
श्रृंग कण्ठ |
उत्तरकाशी – हिमाचल प्रदेश |
|
2 |
थागा ला |
उत्तरकाशी – तिब्बत |
|
3 |
मुलिंग ला (5,669 मीटर) |
उत्तरकाशी – तिब्बत |
|
4 |
माणा (चिरबटिया/डुगरी) ला (5,608 मीटर) |
चमोली – तिब्बत |
|
5 |
नीति (5,044 मीटर) |
चमोली – तिब्बत |
|
6 |
बाराहोती |
चमोली – पिथौरागढ़ |
|
7 |
कुँगरी बिंगरी |
चमोली – तिब्बत |
|
8 |
दारमा |
पिथौरागढ़ – तिब्बत |
|
9 |
लिपुलेख |
पिथौरागढ़ – तिब्बत |
|
10 |
ट्रेल पास |
बागेश्वर – पिथौरागढ़ |
नदियाँ
- गंगा – गोमुख
हिमानी से भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर
गंगा बनती है।
- यमुना – बन्दरपूँछ
क्षेत्र से, मुख्य
सहायक नदियाँ टोंस और गिरिनदी।
- अलकनंदा – देवताल
(जंस्कर श्रेणी) से,
सहायक नदियाँ धवलगंगा, मन्दाकिनी, पिण्डार, भागीरथी।
- पश्चिमी
रामगंगा – दूधातौली
से, कन्नौज
के पास गंगा में मिलती है।
- पूर्वी
रामगंगा – नंदाकोट
से, गोमती
और जकला इसकी सहायक नदियाँ।
- गौरी
गंगा – ऊँटाधुरा
से, काली
गंगा में मिलती है।
- भिलंगना – सहस्त्रताल
से, टिहरी
में भागीरथी में मिलती है।
भाबर प्रदेश
गंगा और शिवालिक श्रेणी के बीच 5–15 मील की सँकरी
पट्टी, रेत-बजरी
और गोल पत्थरों से बनी। जहाँ सिंचाई संभव है, वहाँ मैदानी कृषि होती है।
पहाड़ प्रदेश
1500–7500 फीट
ऊँचा क्षेत्र, तीन
भागों में:
1.
गड्डिया – 1500–2500 फीट
2.
सलाण – 2500–5000 फीट
3.
राठ – 5000–7500 फीट
खनिज – लोहा, ताँबा, जिप्सम, अभ्रक, गंधक, ग्रेफाइट। मुख्य व्यवसाय – कृषि।
भोटान्तिक प्रदेश
महाहिमालय की उत्तरी ढाल से तिब्बत और
रामपुर-बुशहर की सीमा तक। हमेशा हिमाच्छादित, केवल कुछ घाटियों में मौसमी मानव बस्ती।




.jpg)









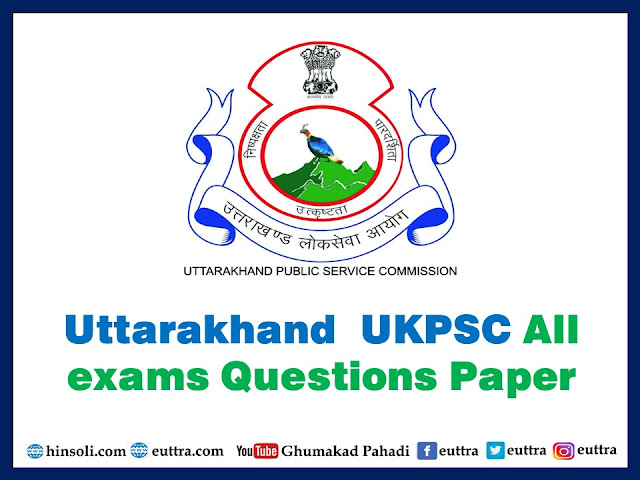







Follow Us